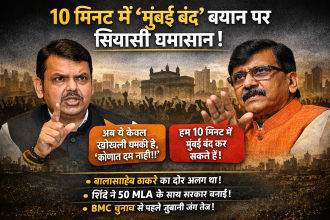भारत में अगली जनगणना कब होगी? | 2026-2027 की जनगणना और जातीय आंकड़ों का महत्व

भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जिसकी सही जनसंख्या और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए हर दस साल में जनगणना की जाती है। यह केवल एक आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर का प्रतिबिंब होती है। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जनगणना की नई तारीखों की घोषणा कर दी है।
यह ब्लॉग भारत में 2026-2027 में होने वाली अगली जनगणना, उसके महत्व, इसमें होने वाले बदलाव और विशेष रूप से जातीय आंकड़ों (Caste Census) को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी देगा।
अगली जनगणना कब होगी?
भारत सरकार के अनुसार अगली जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी:
पहला चरण (Special States):
1 अक्टूबर 2026 से उन राज्यों में शुरू होगा जहाँ भौगोलिक और मौसमी चुनौतियाँ अधिक हैं, जैसे कि:
- जम्मू और कश्मीर
- लद्दाख
- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड
यह चरण इसलिए पहले किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में सर्दी के कारण काम में बाधा आती है।
दूसरा चरण (बाकी भारत):
1 मार्च 2027 से पूरे देश में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल होंगे।
जनगणना का इतिहास
भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश सरकार के समय हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई और तब से हर 10 साल पर यह प्रक्रिया चली आ रही है।
जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत Registrar General and Census Commissioner of India द्वारा कराई जाती है।
जनगणना कैसे होती है?
जनगणना एक दो-चरणीय प्रक्रिया है:
1. हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेन्सस (House Listing):
इसमें देश के हर घर को चिह्नित किया जाता है और उनकी भौतिक स्थिति, सुविधाएं, जल आपूर्ति, शौचालय, बिजली जैसी बुनियादी बातों की जानकारी ली जाती है।
2. जनसंख्या गणना (Population Census):
इसमें हर व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, जैसे:
- नाम
- उम्र
- लिंग
- धर्म
- शिक्षा
- भाषा
- पेशा
- विवाह की स्थिति आदि
इस बार क्या नया होगा?
1. जातीय जनगणना (Caste Census) शामिल:
2026-27 की जनगणना में 93 सालों बाद जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इससे पता चलेगा कि विभिन्न जातियों की संख्या, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार आदि में क्या स्थिति है।
यह क्यों ज़रूरी है?
- सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों की पारदर्शिता के लिए
- पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या जानने के लिए
- योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु
2. डिजिटल जनगणना:
पहली बार जनगणना को डिजिटल रूप से भी किया जाएगा। इसके लिए:
- मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा
- नागरिक स्वेच्छा से Self Enumeration भी कर सकेंगे
3. बहुभाषी विकल्प:
जनगणना फॉर्म्स 16 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे ताकि हर व्यक्ति सही जानकारी दे सके।
जातीय जनगणना: एक ऐतिहासिक कदम
भारत में पिछली बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद से जाति आधारित आंकड़े केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक सीमित रहे। इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य समुदायों की भी गणना की जाएगी।
जातीय जनगणना के लाभ:
| लाभ | विवरण |
| योजनाओं की प्रभावशीलता | जातियों की संख्या और स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकेंगी |
| आरक्षण प्रणाली में सुधार | सटीक आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की समीक्षा संभव |
| शिक्षा और रोजगार नीति | OBC और वंचित वर्गों की सटीक स्थिति सामने आएगी |
| राजनीतिक प्रतिनिधित्व | सीटों के आरक्षण और आवंटन को बेहतर दिशा |
जनगणना क्यों है ज़रूरी?
जनगणना के बिना किसी भी लोकतांत्रिक देश का सही योजना निर्माण संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में यह प्रक्रिया और भी अहम हो जाती है।
मुख्य कारण:
- नीति निर्माण में मदद: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, पेयजल जैसे क्षेत्रों में सही योजनाएं बनाने के लिए जनगणना जरूरी है।
- वित्तीय आवंटन: राज्यों और जिलों को बजट देने में जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल होता है।
- निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण: लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
- शहरीकरण और प्रवास का आकलन: यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है और कहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं।
जनगणना में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:
- व्यक्ति का नाम, लिंग, उम्र
- वैवाहिक स्थिति
- शैक्षणिक योग्यता
- कार्य स्थिति (काम करता है या नहीं)
- व्यवसाय और कार्य स्थल
- भाषा, धर्म और जाति
- दिव्यांगता की स्थिति
- घर के स्वामित्व की स्थिति
- जल, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं
डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता
जनगणना में दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहती है। जनगणना अधिनियम, 1948 के अनुसार:
- किसी भी जानकारी को किसी अन्य सरकारी एजेंसी या अदालत में नहीं बांटा जा सकता।
- कोई भी अधिकारी उस जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
जनगणना को लेकर जनभावनाएं
जनगणना में आम जनता की भागीदारी बेहद ज़रूरी होती है। नागरिकों को चाहिए कि वे सही और पूरी जानकारी दें। कई बार जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक मतभेद और बहसें होती रही हैं, लेकिन इससे मिलने वाले आंकड़े सामाजिक न्याय की बुनियाद बन सकते हैं।
सरकार की तैयारियाँ
सरकार ने सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लगभग 30 लाख कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में लगाया जाएगा। उन्हें डिजिटल डिवाइस और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बजट आवंटन भी बढ़ाया गया है ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो।
निष्कर्ष
भारत की 2026-27 की जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। जातीय आंकड़ों का समावेश इसे और भी अधिक गहन और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
यह जनगणना न केवल सरकार बल्कि समाज के हर वर्ग को बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन देगी। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सटीकता से पूरी की जाती है, तो भारत को सामाजिक न्याय, समानता और विकास के क्षेत्र में नया आयाम मिल सकता है।
आपकी राय क्या है?
क्या आप जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है इससे आरक्षण और योजनाओं में सुधार होगा?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें!